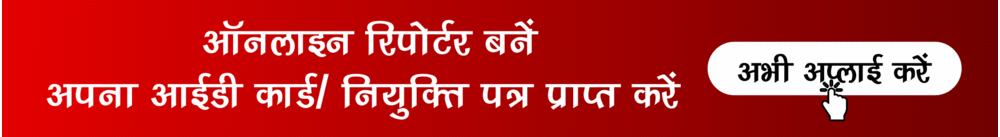रविवारीय विशेष: जब चार कंधे भी भारी पड़ने लगे…

– अवधेश चौकसे
भागदौड़ भरी ज़िंदगी, इंटरनेट की दुनिया और निजी स्वार्थों में डूबते समाज ने हमसे हमारी सबसे बड़ी पहचान छीन ली है — संवेदना।
कभी समाज में ऐसा समय भी था, जब किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होना एक सामाजिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि मानवीय धर्म माना जाता था। अर्थी उठती थी तो मोहल्ला, गली, गाँव उमड़ पड़ता था। श्मशान घाट तक दो-तीन किलोमीटर का रास्ता क्या… पूरा समाज कंधे देने को तत्पर रहता था। कोई किसी से नहीं कहता था, फिर भी कंधे बदलते जाते थे — क्योंकि सबके मन में अपनत्व था, पीड़ा की साझेदारी थी, और सबसे बढ़कर इंसानियत थी।
लेकिन आज?
आज अर्थी उठती है, तो मोहल्ला खाली नज़र आता है। एक-आध रिश्तेदार या पड़ोसी कंधा देते हैं, फिर थककर पीछे हो जाते हैं — क्योंकि आगे कंधा देने को कोई आता ही नहीं। अब मृत्यु पर संवेदना नहीं, सिर्फ औपचारिकता बची है। मानवता अब धीरे-धीरे शव के साथ दफन हो रही है।
ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे नहीं रहे, लेकिन तकनीक, सोशल मीडिया और व्यस्तता ने हमारे भीतर के इंसान को कुंद कर दिया है। दुख में साथ खड़ा होना अब स्टेटस का हिस्सा नहीं रहा। हम “शेयर”, “रील” और “लाइक” में इतने मशगूल हैं कि अंतिम विदाई में शामिल होना अब समय की बर्बादी लगता है।
सोचिए ज़रा…
क्या हम उस दौर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां अंतिम यात्रा में चार कंधे जुटा पाना भी मुश्किल हो जाएगा? क्या समाज अब इतना अकेला हो गया है?
यह चिंता का नहीं, चेतावनी का विषय है।
रिश्ते निभाइए, समाज से जुड़िए, अंतिम यात्रा में शामिल होइए — क्योंकि किसी दिन हम भी वहां होंगे… और तब यही समाज हमें चार कंधे देगा… या नहीं देगा।
विचार कीजिए, क्योंकि संवेदना बची तो समाज बचेगा।