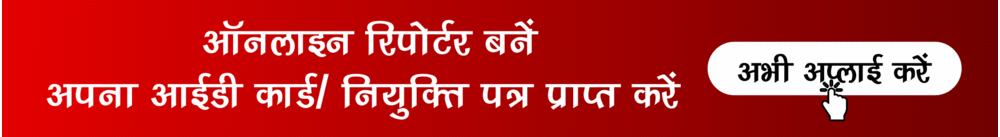समावेशी भाषा के रूप में हिन्दी: हिन्दी दिवस पर आलेख “सुशील शर्मा”
समावेशी भाषा के रूप में हिन्दी: हिन्दी दिवस पर आलेख "सुशील शर्मा"

हिन्दी दिवस पर आलेख “सुशील शर्मा”
भाषा एक सामाजिक क्रिया है, किसी व्यक्ति की कृति नहीं। समाज में यह विचार-विनिमय का साधन है। मनुष्य और मनुष्य के बीच, वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा मानवसभ्यता के विकास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। मानव जाति का सारा ज्ञान भाषा के माध्यम से ही विकसित हुआ है। सृष्टि में केवल मानव ही वाक्शक्ति संपन्न प्राणी है और यही उसकी श्रेष्ठता का मानदण्ड है। मानव वाहे जंगलों में रहता हो या आधुनिक नगरों में, भाषा उसकी सबसे मूल्यवान् सम्पत्ति है। यह कहना अनुचित न होगा कि किसी समाज की भाषा जितनी अधिक समुन्नत होगी उसकी संस्कृति भी उतनी ही अधिक श्रेष्ठ होगी।
विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से भाषा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुये उसे पारिभाषित किया
है। जिन्हे सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में रख सकते हैं-(1) भारतीय (2) पाश्चात्य।
भारतीय मत:-
1. ‘‘वर्णों में व्यक्त वाणी को भाषा कहते है।’’पंतजलि
2. ‘‘भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है।’’ ’ कामता प्रसाद गुरू
3. ‘‘विभिन्न अर्थोें में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है।’’किशोरीदास बाजपेयी
4. डाॅ. बाबूराम सक्सेना ‘‘जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है,उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं।’’
5. डाॅ. मंगलदेव शास्त्री ‘‘भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वाराअपने विचारों को प्रकट करते हैं।’’
6. डाॅ. भोलानाथ तिवारी ‘‘भाषा, उच्चारण अवयवों से उच्चरित, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान
करते हैं।’’
7. पी.डी. गुणे -‘‘शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।’’
8. सुकुमार सेन‘‘अर्थवान, कण्ठ से निःसृत ध्वनि समष्टि ही भाषा है।’’
पाश्चात्य मत:-
प्लेटो ने अपने ग्रंथ याॅपटिक्स’ में एक जगह इस संबंध में कहा है कि
1. ‘‘विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है।’’ तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। –
2. कोचे के अनुसार -अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को भाषा कहते हैं।
3. कार्डिनर के अनुसार (विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं।)
4. ब्लाॅक तथा ट्रेगरके अनुसार भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिससे एक सामाजिक समूह परस्पर सहयोग
करता है।
हिंदी भाषा कीविकास-यात्रा अनेक वीथियों, सरणियों और मार्गों का अनुसरण करती हुई अविराम गति से निरन्तर प्रवाहमान रहकर अपने समूचे परिवेश को आप्लावितऔर रससिक्त करती चलती है।
भारत में द्रविड़ का आगमन आम तौर पर भूमध्यसागरीय नस्लीय जाति की एक शाखा से जुड़ा हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता के उदय से पहले से ही भारत में मौजूद थी। वास्तव में, पुरातत्वविदों का मानना है कि वे प्रोटो-ऑस्ट्रोलोइड्स के साथ-साथ हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। भारत-आर्यन के आगमन से पहले द्रविड़ भाषण समुदाय भारत के अधिकांश उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में पाए गए थे। हालाँकि, उत्तर-पश्चिमी भारत में इंडो-आर्यन के उदय के बाद, एक भाषाई परिवर्तन आया और द्रविड़-भाषी क्षेत्र अपनी भौगोलिक सीमा में सिकुड़ गया
अपभ्रंश में भी इस प्रकार का प्रयोग पाया जाता है, क्यों कि सुखमुखोच्चारण के लिये जन साधारण प्रायः संयुक्त वर्णो के हलन्त वर्णों को सस्वर कर देता है, संस्कृत में इसको युक्तविकर्ष कहते हैं, ऐसे ही शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। धरम, करम, किरपा, हिरदय, अगिन, सनेह आदि ऐसे ही शब्द हैं जो धर्म, कर्म, हृदय, अग्नि, स्नेह के वे रूप हैं जो जनता के मुखों से निकले हैं। अवधी और ब्रजभाषा में ऐसे शब्दों का अधिकांश प्रयोग मिलता है।
अरबी फ़ारसी लिपियों में जो ऐसे वर्ण हैं, जिनका उच्चारण हिन्दी वर्णों के समान है, उनके लिखने में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वरन् फ़ारसी अरबी के कई वर्णों के स्थान पर हिन्दी का एक ही वर्ण प्रायः काम देताहै। परिवर्तन उसी अवस्था में होता है. जब उनमें फ़ारसी अरबी वर्णों से अधिकतर उच्चारण की विभिन्नता पाई जाती है। नीचे कुछ इसका वर्णन किया जाता है।अरबी में कुल २८ अक्षर हैं, इनमें फ़ारसी भाषा के चार विशेष अक्षरों पे, चे, ज़े, गाफ़ के मिलाने से वे ३२ हो जाते हैं। फारसी में एक हे मुग्नफ़ी कहा जाता है. vi):-rj;5-rju-ys के अन्त में जो हे है वही हे मुखफ़ी है । हिन्दी में यह आ हो जाता है जैसे गेज़ा कूज़ा. सबज़ा, जग आदि । कुछ लोगों ने इस हे के स्थान पर विसर्ग लिखना प्रारम्भ किया था. अब भी कोई कोई इसी प्रकार से लिखना पसन्द करते हैं जैसे रोज़ः, कूज़ः, सब्ज़ः, ज़र्र: आदि।
उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसका हिंदी से बहुत गहरा संबंध है, जिसने देश को एक करने में मदद की। यह ज्यादातर उत्तरी भारत में बोली जाती है, जबकि हिंदी भारत के मध्य, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। उर्दू बोलने वाले अधिकांश लोग हिंदुओं के वंशज हैं, हालांकि यह समय के साथ अरबी और फ़ारसी भाषाओं से प्रभावित रहा है।उर्दू भाषा की प्रकृति आज भी हिन्दी है, व्याकरण उसका आज भी हिन्दी प्रणाली में ढला हुआ है, उसमें जो फारसी मुहावरे दाखिल हुए हैं, वे सब हिन्दी रंग में रंगे हैं। फारसी के अनेक शब्द हिन्दी के रूप में आकर उर्दू की क्रिया बन गये हैं। एक बचन बहुधा हिन्दी रूप में बहुवचन होते हैं, फिर उर्दू हिन्दी क्यों नहीं है? यदि कहा जावे फारसी, अरबी, और संस्कृत शब्दों के न्यूनाधिक्य से हो उर्दू हिन्दी का भेद स्थापित होता है, तो यह भी नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्यों कि अनेक उर्दू शायरों का बिल्कुल हिन्दी से लबरेज़ शेर उर्दू माना जाता है, और अनेक हिन्दी कवियों का फ़ारसी और अरबी से लबालब भरा पद्य हिन्दी कहा जाता है। हिन्दी में कुछ फ़ारसी शब्द अधिक मिलगये हैं, और उर्दू नाम करण ने विभेद मात्रा अधिक बढ़ा दी है; तथापि आज तक उर्दू हिन्दी ही है, कतिपय प्रयोगों का रूपान्तर हो सकता है भाषा नहीं बदल सकती। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दी भाषा पर अरबी फ़ारसी और तुर्की शब्दों का इतना अधिक प्रभाव है कि एक विशेष रूप में वह अन्य भाषा सी प्रतीत होती है। ऐसे कई शब्द हैं जो इन दो भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आगे संशोधित किए गए जब वे समुद्री मार्गों के माध्यम से फारस के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के माध्यम से भारतीय पक्ष में पहुंचे। इसके अलावा, उर्दू एक ऐसी भाषा है जो पाकिस्तान में प्रमुख रूप से बोली जाती है, और यही कारण है कि इसे ज्यादातर उत्तरी भारत द्वारा अपनाया गया है।
यदि हम उर्दू पर हिन्दी के प्रभाव की बात करें तो वह हिन्दी पर उर्दू के प्रभाव के बराबर रहा है। प्रभाव परस्पर है, और इसका आदर्श उदाहरण बॉलीवुड है। बॉलीवुड हिंदी के अलावा अपनी फिल्मों में उर्दू के बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा, पाकिस्तान में हिंदी का प्रचलन भी बढ़ा है।
सौ वर्ष के भीतर हिन्दी में बहुत से योरोपियन विशेप कर अंगरेज़ी शब्द भी मिल गये हैं, और दिन दिन मिलते जा रहे हैं। रेल, तार, डाक, मोटर आदि कुछ ऐसे शब्द हैं, जो शुद्ध रूप में ही हिन्दी में व्यवहृत हो रहे हैं, और लालटेन, लम्प आदि कितने ऐसे शब्द हैं, जिन्होंने हिन्दी रूप ग्रहण कर लिया है, और आज कल इनका प्रचार इसी रूप में है। बहुत से सामान पाश्चात्य देशों से भारत वर्ष में ऐसे आ रहे हैं, जिनका हिन्दी नाम है ही नहीं ऐसी अवस्था में उनका योरोपियन अथवा अमरीकन नाम ही प्रचलित हो जाता है। और इस प्रकार उन देशों की भाषा के अनेक शब्द इस समय हिन्दी भाषा में मिलते जा रहे हैं। यह स्वाभाविकता है, विजयी जाति के अनेक शब्द विजित जाति के भाषा में मिल जाते ही हैं, क्यों कि परिस्थिति ऐसा कराती रहती है। किन्तु इससे चिन्तित न होना चाहिये। इससे भाषा पुष्ट और व्यापक होगी, और उसमें अनेक उपयोगी विचार संचित हो जावेंगे।
ऐसा नहीं है कि हिन्दी ने केवल एशियाई या भारतीय भाषाओं को ही प्रभावित किया है; कई अन्य विदेशी भाषाएं भी हैं जो हिंदी से प्रभावित हैं। इसका मुख्य कारण भारत में व्यापार-उन्मुख समुदायों के कारण है जो विदेशों के साथ व्यापार में लगे हुए थे।जिस भाषा में वे आपस में संवाद करते थे वह लोकप्रिय हो गई और अन्य भाषाओं में पहुंचने पर इसे और संशोधित किया गया। इसके अलावा, ऐसे कई शब्द हैं जो हिंदी से उत्पन्न हुए हैं और अंग्रेजी में अपना रास्ता बना चुके हैं, जैसे आम, चूड़ी इत्यादि।हिंदी और विदेशी भाषाओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य यहां दिए गए हैं। जिन देशों में भारतीय आबादी काफी है, वहां स्थानीय भाषा के साथ शब्दों का मिश्रण अपरिहार्य है। इससे इस क्षेत्र में विभिन्न लिंगुआ फ़्रैंक का निर्माण हुआ है।
एक लिंगुआ फ़्रैंका समुदाय द्वारा लोगों के बीच संचार को आसान बनाने के लिए विकसित एक सहायक भाषा है। उदाहरण के लिए, फिजी में, भारतीय हिंदुस्तानी कहे जाने वाले हिंदी और फिजी के शब्दों का मिश्रण बोलते हैं, जिसमें मिश्रण में डाली गई कुछ अंग्रेजी भी शामिल है। यह भाषा अवधी बोली से ली गई है जिसमें मगही, भोजपुरी और बिहारी जैसी विभिन्न भाषाओं का मिश्रण है। फिजी हिंदी भी लिंगुआ फ़्रैंका, कैरेबियन हिंदुस्तानी के समान है।
अगर हम अफ्रीका के बारे में बात करें, तो औपनिवेशिक काल ने कई भारतीयों को गुलाम और नौकर के रूप में अफ्रीका में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। और भारतीयों के अफ्रीका में इस प्रवास के कारण उनकी शब्दावली में विभिन्न शब्द जुड़ गए। आज बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो लंबे समय से अफ्रीकी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने अपने बोलने को काफी प्रभावित किया है। कुछ शब्दावली शब्दों जैसे स्वाहिली या सोमाली का उपयोग अफ्रीका के भारतीयों में मूल निवासियों से बात करने के लिए सामान्य है।
भाषाओं के संपर्क में आकर, उनसे बहुत कुछ ग्रहण करके और अहिन्दी भाषियों द्वारा प्रयुक्त होते-होते उसका यथासमय एक सर्वसम्मत अखिल भारतीय रूप
विकसित होगा। फिर लेखन, टंकण और मुद्रण के क्षेत्र में तो हिन्दी भाषा में एकरूपता बहुत जरूरी है ताकि उसका एक विशिष्ट स्वरूप निश्चित हो सके।
आज के यंत्राधीन जीवन को देखते हुए यह अनिवार्य भी है।यह भी सच है कि भाषा-विषयक कठोर नियम बना देने से उनकी स्वीकार्यता तो संदेहास्पद हो ही जाती है, साथ ही भाषा के स्वाभाविक विकास में भी अवरोध आने का थोड़ा-सा डर रहता है। फलतः भाषा गतिशील, जीवन्तऔर समयानुरूप नहीं रह पाती।